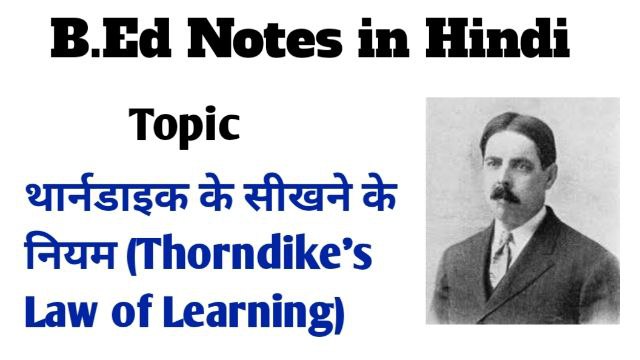थार्नडाइक के सीखने के नियम (THORNDIKE’S LAWS OF LEARNING)
बहुत समय से अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, पशुओं पर परीक्षण करके ‘सीखने’ के नियमों की खोज में लगे हुये हैं। उन्होंने सीखने के जो नियम प्रतिपादित किये हैं, उनमें सबसे अधिक मान्यता ई. एल. थार्नडाइक (E. L. Thorndike) के नियमों को दी जाती है। उसने सीखने के नियमों को दो भागों में बाँटा है-
(क) सीखने के मुख्य नियम, (ख) सीखने के गौण नियम।
क) सीखने के मुख्य नियम (Primary Laws of Learning)
सीखने के मुख्य तीन नियम इस प्रकार है-
1) तत्परता का नियम (Law of Readiness)-
इस नियम के अनुसार व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने के बाद ही सीख सकता है। सीखने के लिए तत्पर रहने से अधिगम शीघ्र व स्थायी होता है। तत्परता व्यक्ति को ध्यान केन्द्रित करने में योगदान देती है जिससे क्रिया आसानी से सम्पन्न हो जाती है। मानसिक रूप से तैयार न होने पर कोई भी कार्य और व्यवहार कष्टदायक होता है। भाटिया के अनुसार, ‘तत्पर होना मतलब किसी कार्य को आधा कर लेना।
2) अभ्यास का नियम (Law of Exercise)-
इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार-बार करने या दोहराने से वह याद हो जाती है और छोड़ देने पर या न दोहराने पर वह भूल जाती है। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग न करने पर आधारित है। उदाहरणार्थ, कविता और पहाड़े याद करने के लिए उन्हें बार-बार दोहराना पड़ता है तथा अभ्यास के साथ-साथ उपयोग में भी लाना पड़ता है। ऐसा करने पर सीखा हुआ कार्य भूलने लगता है। उदाहरणार्थ, याद की गई कविता को कभी न सुनाया जाये तो वह धीरे-धीरे भूलने लगती है। यही बात साइकिल चलाना, टाइप करना, संगीत आदि में भी लागू है।
थार्नडाइक के अनुसार, अभ्यास के नियम के अन्तर्गत दो उपनियम आते हैं- (i) उपयोग का नियम, (ii) अनुपयोग का नियम।
(i) उपयोग का नियम (Law of Use)-
इस नियम का तात्पर्य है- अभ्यास कुशल बनाता है (Prac- tice Makes Perfect)। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो हम उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। हम बिना अभ्यास किये साइकिल पर चढ़ने में या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो सकते।
(ii) अनुपयोग का नियम (Law of Disuse)-
इस नियम का अर्थ यह है कि यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। अभ्यास के माध्यम से ही हम उसे स्मरण रख सकते हैं। डगलस व हॉलैण्ड का कथन है- “जो कार्य बहुत समय तक किया या दोहराया नहीं जाता है वह भूल जाता है। इसी को अनाभ्यास का नियम कहते हैं।
3) प्रभाव का नियम (Law of Effect)-
थार्नडाइक का यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है। इस नियम को ‘सन्तोष असन्तोष’ का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार, जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं और जिसमें सुख और सन्तोष प्राप्त होता है, उसी को व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने से कष्ट होता है, दुःखद फल प्राप्त होता है, उसे व्यक्ति नहीं दोहराता है। इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसे लाभ मिलता है तथा सन्तोष प्राप्त होता है। संक्षेप में, जिस कार्य के करने से पुरस्कार मिलता है उसे सीखते हैं और जिस कार्य के करने से दण्ड मिलता है उसे नहीं सीखा जाता।
Read Also- थार्नडाइक का सीखने का सिद्धान्त | प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत
(ख) सीखने के गौण नियम (Secondary Laws)
सीखने के गौण नियम इस प्रकार हैं-
(1) बहु-प्रतिक्रिया का नियम (Law of Multi-Response)-
जब व्यक्ति कोई बात सीखता है तो वह अपनी मूल प्रवृत्तियों या पहले सीखी हुई बातों के आधार पर विविध प्रकार की कई अनुक्रियाएँ करता है। इन्हीं क्रियाओं में से जब वह ठीक क्रिया पर पहुँचता है तब उसे सफलता मिल जाती है। सीखने वाला तब तक क्रियाएँ बदलता रहता है, जब तक वह ठीक क्रिया पर नहीं पहुँच जाता है। यदि बहु-अनुक्रियाएँ नहीं होगी तो सीखने वाला ठीक क्रिया पर नहीं पहुँच पायेगा। ‘प्रयत्न और भूल’ द्वारा ‘सीखने का सिद्धान्त’ इसी नियम पर आधारित है।
(2) मनोवृत्ति का नियम (Law of Disposition) –
इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं तो या तो हम उसे करने में असफल होते हैं या अनेक त्रुटियाँ करते हैं। यही कारण है कि शिक्षक प्रेरणा देकर बालकों को नवीन ज्ञान को ग्रहण के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं।
(3) आंशिक क्रिया का नियम (Law of Partial Activity) –
किसी कार्य को करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि सम्पूर्ण कार्य को एक बार में न करके उसको भागों में विभाजित करके किया जाये। इसे अंशों में विभाजित करके सीखना कहते हैं। कार्य का विभाजन कार्य को सरल बना देता है। यदि किसी कविता को अंशों में विभाजित करके याद किया जाये तो याद करने में सुविधा हो जाती है। इसी नियम के आधर पर ‘अंश से पूर्ण की ओर’ शिक्षण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसमें शिक्षक अपनी सम्पूर्ण विषय-सामग्री को छोटे-छोटे खण्डों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है।
(4) आत्मीकरण का नियम (Law of Assimilation)-
जब व्यक्ति के सामने कोई नवीन परिस्थिति आती है और यह परिस्थिति किसी पूर्व परिस्थति के समान होती है तो व्यक्ति की अनुक्रियाएँ वैसी ही होंगी, जैसी कि वे पहली परिस्थिति के समय थीं। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति नवीन ज्ञान को ग्रहण पूर्व ज्ञान के आधार पर करता है। यही आत्मीकरण का नियम है। दूसरे शब्दों में, हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। यही कारण है कि जब शिक्षक बालक को कोई नई बात सिखाता है, तब उसका पहले सीखी हुई बात से सम्बन्ध स्थापित कर देता है।
(5) सम्बन्धित परिवर्तन का नियम (Law of Associative Shifting)-
इस नियम का तात्पर्य यह है कि सीखने वाले व्यक्ति की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तन होता है अर्थात् पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना। इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है, पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ, प्रेमिका की अनुपस्थिति में प्रेमी उसके चित्र से उसी प्रकार बातें करता है जिस प्रकार वह उससे करता था।