इस लेख में भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला का वर्णन (Bharat ki Pragaitihasik Chitrakala ka vernan) के अंतर्गत परिचय, प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ, उत्पत्ति, प्रमुख कालखंड (प्रारंभिक, मध्य, नवपाषाण युग), रंग व तकनीक, विषयवस्तु, प्रमुख स्थल (भीमबेटका, लखुदियार आदि), कलात्मक विशेषताएँ, महत्व, संरक्षण और निष्कर्ष शामिल हैं। इसे पढ़कर हम प्राचीन मानव की जीवनशैली, कला-बोध, धार्मिक आस्था, सामाजिक संगठन और भारतीय चित्रकला की जड़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
परिचय
भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण कलात्मक धरोहर है। यह उस काल की अभिव्यक्ति है जब मनुष्य ने अभी लेखन प्रणाली का विकास नहीं किया था। उस समय मनुष्य अपने अनुभवों, भावनाओं, विश्वासों और जीवनशैली को व्यक्त करने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। उसने गुफाओं और चट्टानों की दीवारों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इन चित्रों में उसके जीवन के विविध पहलू दिखाई देते हैं—जैसे शिकार, नृत्य, पशुपालन, सामाजिक संगठन, धार्मिक विश्वास और प्रकृति से जुड़ाव। इन चित्रों के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि प्रारंभिक मनुष्य केवल जीवित रहने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसमें सौंदर्यबोध और कलात्मक चेतना भी थी।
‘प्रागैतिहासिक’ शब्द का अर्थ
‘प्रागैतिहासिक’ शब्द का अर्थ है—ऐसा समय जो इतिहास के लिखित प्रमाणों से पहले का है, अर्थात जब मनुष्य ने लेखन कला का आविष्कार नहीं किया था। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के औजार बनाए, गुफाओं में निवास किया और शिकार, संग्रह तथा पशुपालन के माध्यम से जीवन यापन किया। इस काल को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है—प्रारंभिक पाषाण युग (Paleolithic Age), मध्य पाषाण युग (Mesolithic Age) और नवपाषाण युग (Neolithic Age)। इन तीनों युगों के दौरान चट्टानों पर बनाए गए चित्र ही प्रागैतिहासिक चित्रकला कहलाते हैं।
- खजुराहो के मंदिरों की स्थापत्य विशेषताएं | Khajuraho ke mandiro ki vishestaye B.A 3rd Year Notes
- रांके द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ और उनका महत्व B.A 3rd Year Notes
- टॉयनबी के अनुसार सभ्यता के उत्थान एवं पतन की प्रक्रिया B.A 3rd year Notes
भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्भव
भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की शैलाश्रयों से प्राप्त हुआ है। यहाँ लगभग 700 से अधिक शैलाश्रय हैं, जिनमें से लगभग 400 में चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। इन चित्रों में अनेक कालखंडों की कलात्मक परंपराएँ झलकती हैं। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
भीमबेटका के अतिरिक्त भारत में अन्य कई स्थलों से भी प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, जैसे—मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का आदमगढ़, उत्तराखंड का लखुदियार, झारखंड का कुण्डा, छत्तीसगढ़ का ग्वाराटोली, बिहार की बरबार गुफाएँ, कर्नाटक का बेल्लारी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का कोंडापल्ली। ये सभी स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक मानव की सृजनशीलता के साक्ष्य हैं।
प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख कालखंड
- प्रारंभिक पाषाण युग (Palaeolithic Age) – 40,000 ई.पू. से 10,000 ई.पू.
यह प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रारंभिक चरण है। इस युग के चित्र सरल, सीमित रंगों वाले और छोटे आकार के होते थे। विषय मुख्यतः शिकार से संबंधित थे। लाल और गेरुए रंगों से पशुओं, शिकारी समूहों और दैनिक जीवन के दृश्य बनाए गए। आकृतियाँ रेखाओं पर आधारित और प्रतीकात्मक थीं। भीमबेटका की “गाय और भैंस का शिकार” जैसी चित्रकृतियाँ इस काल की प्रमुख उदाहरण हैं।
- मध्य पाषाण युग (Mesolithic Age) – 10,000 ई.पू. से 4,000 ई.पू.
यह युग प्रागैतिहासिक चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। इस समय सामाजिक जीवन, सामूहिक क्रियाओं और उत्सवों का चित्रण हुआ। रंगों में विविधता—लाल, पीला, सफेद, हरा—दिखाई देती है। चित्रों में गति और लय है। नृत्य, युद्ध, शिकार और संगीत के दृश्य सामान्य हैं। भीमबेटका की “नृत्य दृश्य” और “शिकार दृश्य” प्रसिद्ध उदाहरण हैं।
- नवपाषाण युग (Neolithic Age) – 4000 ई.पू. से 1800 ई.पू.
इस काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक बन गया। चित्रों में कृषि, पशुपालन, सामाजिक जीवन और धार्मिक प्रतीकों का चित्रण हुआ। ज्यामितीय आकृतियाँ और प्रतीक विचारशीलता व आध्यात्मिकता का संकेत हैं। आदमगढ़ की “बैलगाड़ी और खेत” संबंधी चित्रकृति इस युग की विशिष्ट रचना है।
रंग और सामग्री
प्रागैतिहासिक कलाकारों ने प्राकृतिक स्रोतों से रंग बनाए।
लाल रंग – गेरू या आयरन ऑक्साइड से
सफेद रंग – चूना पत्थर या राख से
काला रंग – लकड़ी की कालिख या चारकोल से
पीला रंग – मिट्टी या पौधों के रस से
इन रंगों को पशु वसा, वनस्पति रस या पानी में मिलाकर टिकाऊ बनाया जाता था। चित्र गुफाओं की दीवारों और छतों पर बनाए जाते थे ताकि सूर्य की सीधी किरणों से उनकी सुरक्षा हो सके।
चित्रण तकनीक
कलाकार उँगलियों, लकड़ी की टहनियों, पशु बालों के ब्रश या पक्षियों के पंखों से चित्र बनाते थे। वे पहले रेखांकन करते और फिर रंग भरते थे। रेखाओं की मोटाई और दिशा से गति, भाव और ऊर्जा प्रदर्शित की जाती थी। कभी-कभी पुराने चित्रों के ऊपर नए चित्र बनाए जाते थे, जिससे परतें बन जाती थीं।
विषयवस्तु
शिकार दृश्य सबसे अधिक चित्र शिकार से संबंधित हैं। इनमें पुरुष समूहों को हिरण, भैंस या जंगली सूअर का शिकार करते दिखाया गया है।
नृत्य और संगीत
कई चित्र सामूहिक नृत्य और संगीत को दर्शाते हैं। इससे पता चलता है कि लोग सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर उत्सव मनाते थे।
पशु चित्र
बाघ, हाथी, घोड़ा, हिरण, भैंस, बकरी आदि के चित्र प्रमुख हैं। कुछ चित्रों में पशु पूजनीय रूप में भी दर्शाए गए हैं। दैनिक जीवन और प्रतीकात्मक चित्र स्त्रियों के गृहकार्य, बच्चों के खेल, कृषि कार्य, सूर्य, चंद्रमा, वृत्त, त्रिकोण आदि आकृतियों के प्रतीकात्मक चित्र भी मिलते हैं।
प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख स्थल
भीमबेटका
यह भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ के चित्रों में शिकार, नृत्य, युद्ध और धार्मिक अनुष्ठान के दृश्य हैं। “नृत्य करते समूह”, “हिरण का शिकार” और “घोड़े पर सवार योद्धा” प्रमुख उदाहरण हैं।
लखुदियार
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित लखुदियार गुफाओं में मानव आकृतियाँ, पशु, नृत्य और शिकार के दृश्य हैं। लाल, सफेद और काले रंगों का प्रयोग हुआ है। “मानवों का सामूहिक नृत्य” यहाँ की प्रसिद्ध चित्रकृति है।
अन्य स्थल
आदमगढ़ (म.प्र.) – खेतों और बैलगाड़ी के चित्र
कुण्डा (झारखंड) – पशुपालन के दृश्य
बेल्लारी (कर्नाटक) – शिकार और नृत्य दृश्य
ग्वाराटोली (छत्तीसगढ़) – प्रतीकात्मक चित्र
कोंडापल्ली (आंध्र प्रदेश) – धार्मिक अनुष्ठानों के दृश्य
भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषताएँ (Characteristics)
- सरलता और स्वाभाविकता – चित्रों में अत्यधिक सादगी है, आकृतियाँ रेखाओं और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त की गई हैं।
- सीमित रंग प्रयोग – लाल, गेरुआ, सफेद और काले रंगों का प्रमुख प्रयोग किया गया।
- सजीवता और गतिशीलता – आकृतियों में गति, लय और जीवन्तता स्पष्ट है।
- प्रकृति के प्रति लगाव – पशु, पेड़, जल, पर्वत आदि का बार-बार चित्रण हुआ।
- सामूहिक जीवन की झलक – नृत्य, उत्सव और शिकार जैसे समूह दृश्यों से सामाजिक एकता प्रकट होती है।
- धार्मिक और प्रतीकात्मक तत्व – सूर्य, चंद्रमा, वृत्त, त्रिकोण आदि आकृतियाँ धार्मिक या प्रतीकात्मक अर्थ लिए हैं।
- प्रयोगशीलता और सृजनात्मकता – कलाकारों ने प्राकृतिक रंगों और उपकरणों से प्रभावशाली अभिव्यक्ति दी।
- परतदार चित्रण – एक ही दीवार पर विभिन्न कालों के चित्रों की परतें दिखाई देती हैं।
- आध्यात्मिकता और विचारशीलता – विशेष रूप से नवपाषाण युग के चित्रों में।
- भारतीय कला परंपरा की जड़ें – बाद की अजंता-बाघ चित्रकला पर इसका प्रभाव स्पष्ट है।
संरक्षण की समस्या
समय, जलवायु, वर्षा, धूप और मानव हस्तक्षेप से इन चित्रों की रंगत फीकी पड़ रही है। पर्यटन, प्रदूषण और प्राकृतिक क्षरण ने भी नुकसान पहुँचाया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और यूनेस्को इनकी सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं।
निष्कर्ष
भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला केवल कला का उदाहरण नहीं, बल्कि यह मानव सभ्यता के आरंभिक मानसिक और सांस्कृतिक विकास की साक्षी है। यह बताती है कि प्रारंभिक मनुष्य में सौंदर्यबोध, संवेदना और अभिव्यक्ति की भावना थी। भीमबेटका, लखुदियार और आदमगढ़ जैसे स्थल हमें दिखाते हैं कि कला मानव की मूल प्रवृत्ति है। इन धरोहरों को सुरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मानवता की सबसे प्राचीन और सुंदर अभिव्यक्तियाँ हैं।

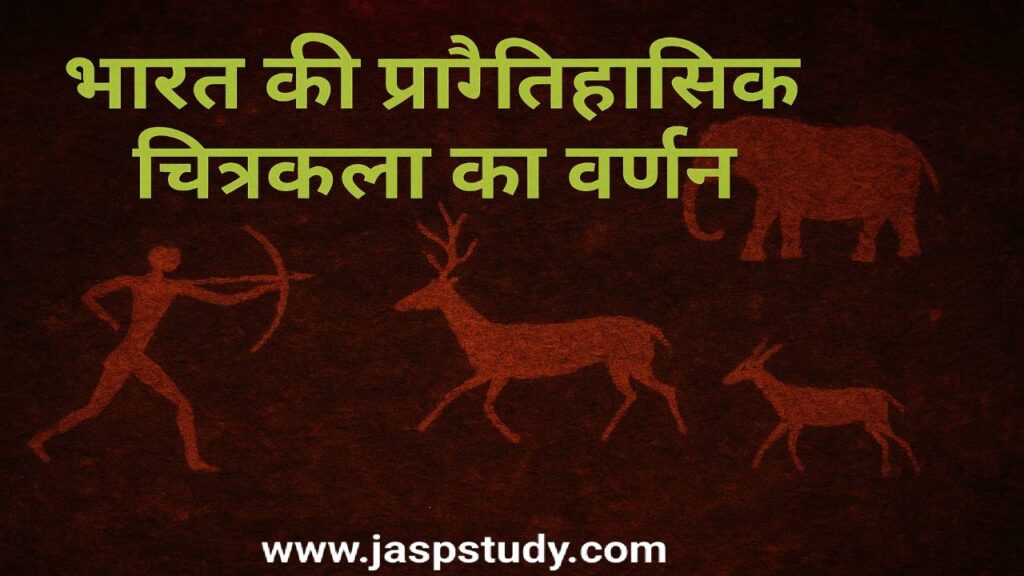
Great wordpress blog here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! take care