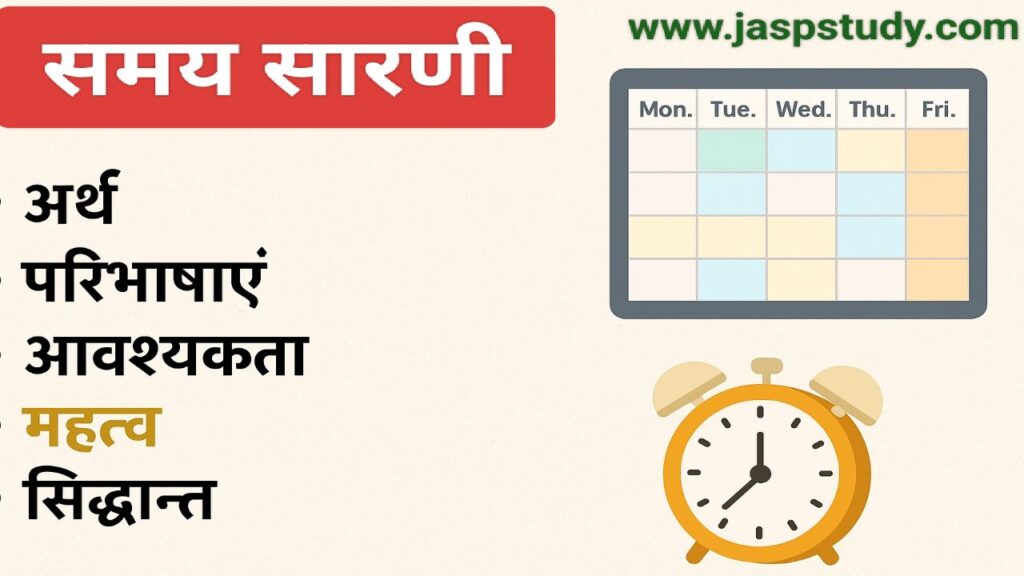इस लेख समय सारणी का अर्थ,परिभाषाएँ,प्रकार,आवश्यकता,महत्व,सिद्धांत|Completet time table notes in hindi में विद्यालय की समय-सारणी का अर्थ, परिभाषाएँ, प्रकार, आवश्यकता, महत्त्व तथा निर्माण के सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि समय-सारणी विद्यालय के सुचारु संचालन, अनुशासन, कार्य-कुशलता और समय प्रबंधन के लिए कितनी आवश्यक है। इस लेख को पढ़कर समय-सारणी के संगठनात्मक, शैक्षिक एवं नैतिक महत्त्व की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह नोट्स प्रमाणिक पुस्तकों से संकलित है।
समय सारणी का अर्थ (Meaning of Time Table)
विद्यालय समय सारणी विद्यालय का एक आवश्यक अंग होती है। यह एक दर्पण के समान होती है जिसके माध्यम से विद्यालय के समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों की एक झलक मिलती है। समय-सारणी के माध्यम से शिक्षक एवं छात्रों को अपने कार्यों के विषय में सूचनाएँ प्राप्त होती हैं।
समय सारणी से तात्पर्य शिक्षक व अन्य गतिविधियों की एक सुनियोजित एवं विधिवत् तैयार की गई योजना से है। समय सारणी एक लेखा होती है जिसके माध्यम से विद्यालय के दैनिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है। यह विभिन्न कक्षाओं, गतिविधियों व विषयों में प्रतिदिन समय विभाजन की योजना ही समय-सारणी कहलाती है।
परिभाषाएँ
डॉ जसवन्त सिंह के अनुसार, ‘समय-सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं एवं उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है।”
एस. के. कोचर ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है- ‘विद्यालय की जिस योजना या चार्ट के द्वारा प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, क्रियाओं के मध्य प्रदर्शित किया जाता है, उसे समय सारणी कहते हैं।
एच. जी. स्टैंड (H. G. Stead) के अनुसार, ‘यह समय सारणी ही है जो कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिसके अनुसार विद्यालय का कार्य होता है। यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से विद्यालय का उद्देश्य एवं लक्ष्य सम्पादित होता है।”
- अच्छे विद्यालय भवन की विशेषताएं B.Ed Notes|Characteristics of Good School Buliding in Hindi
- मूल्य शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता ,उद्देश्य और मूल्यों के प्रकार
- Complete B.Ed Notes in Hindi
- Group Dynamics in hindi – Meaning,Definition B.Ed Notes
- वृद्धि और विकास का अर्थ,अंतर,प्रभावित करने वाले कारक B.Ed Notes
- विस्मृति का अर्थ ,परिभाषा, प्रकार,कारण,उपाय और महत्व B.Ed Notes
- स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धान्त| Skinner’s Theory of Operant Conditioning in hindi B.Ed Notes
- समायोजन की रक्षा युक्तियाँ | Defense Mechanisms of Adjustment in hindi B.Ed Notes
समय-तालिका के प्रकार (Types of Time Table)
(1) सामान्य समय-तालिका,
(2) कक्षा समय तालिका,
(3) अध्यापक समय-तालिका,
(4) खाली घण्टों की समय-तालिका,
(5) पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की समय तालिका,
(6) गृहकार्य की समय-तालिका,
(7) खेल की समय तालिका
सामान्य समय-तालिका (General Time-Table)
इस समय तालिका को मुख्य समय-तालिका या प्रधान समय तालिका भी कहते हैं। यह समय तालिका पूरे विद्यालय की समस्त गतिविधियों को संयुक्त रूप में प्रदर्शित करती है। अतः इसे संयुक्त समय तालिका भी कह सकते हैं। इस समय तालिका में प्रत्येक कक्षा, प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक घण्टे के दैनिक क्रियाकलापों का वर्णन होता है।
अतः इस समय तालिका से ही प्रत्येक कक्षा की, प्रत्येक शिक्षक की, खाली घण्टों की तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की समय-तालिका का निर्माण किया जाता है। इस समय तालिका को प्रधानाध्यापक के कक्ष में रखा जाता है क्योंकि यह प्रधानाध्यापक के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसकी सहायता से प्रधानाध्यापक या अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी भी समय विद्यालय की समस्त गतिविधियों से परिचित हो सकते हैं।
कक्षा समय-तालिका (Class Time-Table)
यह समय तालिका प्रत्येक कक्षा उपवर्ग (Section) के लिये बनायी जाती है। इसका निर्माण सामान्य समय तालिका के आधार पर किया जाता है। इससे यह विदित होता है कि अमुक कक्षा उपवर्ग में कौन सा विषय किस अध्यापक द्वारा किस-किस दिन पढ़ाया जा रहा है। अतः इस समय तालिका द्वारा केवल एक कक्षा उपवर्ग की गतिविधियों का विवरण मिलता है।
अध्यापक समय-तालिका (Teacher’s Time-Table)
अध्यापक समय तालिका से यह अभिप्राय होता है कि प्रत्येक अध्यापक की किस कक्षा में किस समय कक्षाएं हैं और उसे कौन सा विषय पढ़ाना है। अतः इस तालिका द्वारा प्रत्येक अध्यापक को अपनी व्यक्तिगत समय तालिका का पता लगता है। अतः इसकी एक प्रतिलिपि अध्यापक के पास रहती है। इस समय तालिका का निर्माण भी सामान्य समय-तालिका के आधार पर ही किया जाता है। सब शिक्षकों की समय-तालिकाओं को संयुक्त करके एक तालिका बनायी जा सकती है जिसकी एक प्रतिलिपि प्रधानअध्यापक के पास तथा एक प्रतिलिपि स्टाफ-कक्ष में रखी जाती है।
ये समय तालिका दो प्रकार की हो सकती है-
(अ) अध्यापक संयुक्त समय-तालिका
(ब) अध्यापक (व्यक्तिगत) समय तालिका
(अ) अध्यापक संयुक्त समय तालिका – इसमें सारे शिक्षकों के कार्यक्रमों का विवरण संयुक्त रूप में दिया जाता है। इसमें शिक्षक के कुल कार्यभार तथा खाली समय का विवरण स्वयं स्पष्ट हो जाता है।
(ब) अध्यापक (व्यक्तिगत) समय तालिका – इस समय तालिका का निर्माण संयुक्त अध्यापक समय तालिका से किया जाता है। इसकी प्रतिलिपि प्रत्येक शिक्षक अपने पास रखता है।
खाली घण्टों की समय-तालिका (Vacant Periods Time-Table)
इस समय तालिका की मुख्य विशेषता यह है कि यह शिक्षकों के खाली घण्टों के बारे में सूचना देती है। इससे यह पता लगता है कि कौन सा अध्यापक किस घण्टे में खाली है। इस समय तालिका का निर्माण भी सामान्य समय तालिका के आधार पर ही होता है। इस समय तालिका को बनाने का मुख्य प्रयोजन यह है कि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक को उसके खाली घण्टों में कोई अतिरिक्त काम दिया जा सके। जैसे प्रायः दो-तीन शिक्षकों के एक साथ अवकाश ले लेने से विद्यालय की व्यवस्था के लिये शिक्षकों को कुछ अतिरिक्त कक्षाएं अस्थायी रूप से दे दी जाती हैं। इससे विद्यालय का अनुशासन बिगड़ने नहीं पाता है।
पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की समय तालिका(Co-curricular Activities Time-Table)
पाठ्यक्रम क्रियाओं के आयोजन के साथ-साथ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन भी एक विद्यालय के लिये आवश्यक होता है। अतः प्रत्येक विद्यालय को इनके आयोजन के बारे में पूर्वयोजना बनानी पड़ती है जिससे इनकी व्यवस्था समुचित ढंग से सही समय पर हो सके। अतः विद्यालय में सत्र के प्रारम्भ होते समय पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं सम्बन्धी सूची तैयार करनी पड़ती है। साथ ही यह भी निश्चित करना पड़ता है कि इनका आयोजन शिक्षक द्वारा कहां और कब होगा। अतः इस तालिका में पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया का नाम, प्रभारी शिक्षक का नाम तथा समय लिख दिया जाता है।
खेल सम्बन्धी समय तालिका (Games Time-Table)
खेल सम्बन्धी समय तालिका का निर्माण विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं किया जाता बल्कि खेल का शिक्षक इस समय तालिका का निर्माण अपनी सुविधानुसार करता है। खेल का शिक्षक बालकों की उम्र, क्षमता एवं रुचि के अनुसार विद्यार्थियों को अलग-अलग समूहों में विभाजित करता है और यह निश्चित करता है कि किस दिन कौन से समूह को कौन सा खेल या अभ्यास करना होगा। इस तालिका के निर्माण में विद्यालय में उपलब्ध संसाधन एवं खेल का मैदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
गृहकार्य की समय-तालिका (Home Work Time-Table)
कक्षा में शिक्षण के बाद बच्चे के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति हेतु बच्चों को घर से करने के लिये काम दिया जाता है। प्रायः देखने में यह आता है कि किसी दिन तो बच्चे को बहुत अधिक काम मिल जाता है और किसी दिन किसी भी विषय में काम नहीं मिलता है। अतः गृह कार्य को भी पूर्व नियोजित करने से प्रत्येक दिन बच्चों को बराबर गृह-कार्य दिया जा सकता है। अतः इस समय तालिका में यह निश्चित किया जाता है कि किस कक्षा को किसी दिन कितने विषयों में गृहकार्य दिया जायेगा।
समय सारणी की आवश्यकता (Need of TimeTable)
समय सारणी की आवश्यकता को निम्न बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है-
1) अधिकारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है (Fulfil the Needs of Administrators)
समय-सारणी विद्यालय एवं अधिकारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसलिए समय सारणी तैयार करते समय सम्बन्धित अधिकारियों के हितों की अनदेखी व उल्लंघन न हो पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
2) समय-सारणी द्वारा विद्यालय काय सुचारु रूप से चलता है (School Work Runs Smoothly and Orderly Through Time Table)
समय-सारणी में सभी बातें पूर्णतः कल्पित होती है। यह बालक-बालिकाओं एवं शिक्षकों को निर्धारित समय का ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में भी समय-सारणी की सहायता से विद्यालय सुचारु रूप से चलाया जा सकता है जबकि इसके अभाव में समस्त कार्य अस्त-व्यस्त हो जाता है। यही कारण है कि सभी विद्यालयों में इसे योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जाता है।
3) छात्रों में अध्ययन के प्रति उत्साह (Enthusiasm in Students Towards Study)
वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत समय-सारणी के निर्माण में बालकों की रुचियों, योग्यताओं, दृष्टिकोणों तथा बौद्धिक क्षमताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा विषयों के अध्ययन का समय इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि छात्र थकावट अनुभव न करे तथा थकावट होने पर उन्हें समुचित विश्राम प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की व्यवस्था के परिणामस्वरूप छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि तथा उत्साह बढ़ता है।
4) समय तथा ऊर्जा की बचत (Time and Energy Saving)
किस कार्य को किस समय करना है इस बात का ज्ञान हमें समय सारणी कराती है। यह एक ही समय में शिक्षक एवं छात्रों का ध्यान आकर्षित करती है। इस प्रकार समुचित ध्यान के आकर्षण के कारण समय तथा ऊर्जा की बचत होती है। यदि इसका प्रयोग उचित ढंग से किया जाए तो भ्रान्ति, अक्षमता एवं पुनरावृत्ति जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है।
5) कार्य-कुशलता में वृद्धि (Improvement in Efficiency)
समय-सारणी शिक्षकों तथा छात्रों दोनों की कुशलता में वृद्धि होती है। दोनों शिक्षण-प्रक्रिया द्वारा अपने-अपने कार्य को निश्चित समय में पूरा करने के लिए नियमित रूप से कार्य करते हैं। उन्हें अपना कार्य बोझिल प्रतीत नहीं होता है तथा वे उसे पूर्ण करने में रुचि एवं उत्साह प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार दोनों में नियमित तथा रूचि पूर्वक कार्य की आदत का विकास होता है। जिससे उनकी कार्य कुशलता में धीरे-धीरे वृद्धि होती चली जाती है।
6) प्रत्येक विषय एवं क्रिया पर यथेष्ट ध्यान (Ensures Due Attention to Every Subject and Activity)
समय-सारणी के निर्माण में प्रत्येक विषय तथा क्रिया पर यथेष्ट ध्यान दिया जाता है ताकि कोई विषय या क्रिया का अध्यापन या अध्ययन रह न जाए। विषयों के महत्त्व तथा कठिनता पर भी समुचित ध्यान दिया जाता है ताकि इस प्रकार के अध्यापन के घण्टे नियुक्त किए जा सके एवं सभी विषयों का उनके सापेक्षित महत्त्व के अनुसार शिक्षण हो सके।
7) नैतिक मूल्यों का विकास (Development of Moral Values)
समय-सारणी छात्रों तथा शिक्षकों में नैतिक मूल्यों का भी विकास करती है। इसके द्वारा कार्य करने से शिक्षकों तथा छात्रों में यथाविधि करने की आदत का विकास हो जाता है। वे कार्य, समय, नियम, उत्तरदायित्व आदि के महत्त्व को समझने लगते हैं ताकि उनमें नैतिक दृढ़ता ही वृद्धि होती है।
8) विद्यालय जीवन में व्यवस्था तथा अनुशासन (Order and Discipline in School Life)
समय-सारणी विद्यालय की रीढ़ होती है। इसके द्वारा छात्रों में अनुशासन की स्थापना में भी सहयोग मिलता है। समय-सारणी के लागू होते ही शिक्षक, छात्र तथा अन्य कर्मचारी भी अपने-अपने काम में व्यस्त हो जाते है जिससे अनुशासन हीनता की सम्भावना नहीं रहती है। इस प्रकार समय सारणी विद्यालय को गति एवं अनुशासन देती है जिसके चलते विद्यालय निःसन्देह उन्नति के पथ पर अग्रसर रहता है।
9) मनोवैज्ञानिक महत्त्व (Psychological Importance)
परीक्षा के बाल केन्द्रित होने के कारण समय-सारणी को भी बाल केन्द्रित अर्थात् बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं आदि के अनुकूल बनाया जाता है। इस दृष्टि से समय-सारणी में बालकों की थकान, खाने-पीने, उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास के लिए विभिन्न क्रियाओं का आयोजन आदि के लिए उचित समय प्रदान किया जाता है।
समय-सारणी का महत्त्व (Importance of Time Table)
समय-सारणी का महत्त्व निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट होता है-
(1) विद्यालय कार्यक्रमों का ज्ञान – समय-सारणी से विद्यालय के अनेक कार्यक्रमों का ज्ञान होता है। इससे पता चलता है कि विद्यालय में कौन-कौनसे पाठ्यक्रम हैं, कौन-कौन-सी सहगामी तथा शारीरिक क्रियाएँ चलती है, खेलकूद की क्या व्यवस्था है तथा प्रत्येक क्रिया को कितना समय दिया जाता है ?
(2) समय एवं श्रम का सदुपयोग – समय-सारणी के द्वारा विद्यालय के समस्त मानवीय एवं भौतिक साधनों का सुन्दर समन्वय किया जाता है। इस समन्वय के समस्त साधनों का अधिकतम उपयोग कम से कम व्यय पर सम्भव होता है। इससे समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है।
(3) कार्य-कुशलता में वृद्धि – समय-सारणी के द्वारा सभी कार्य नियमित समय पर कराये जाते हैं। प्रधानाध्यापक, अध्यापक तथा छात्र सभी जानते हैं कि उन्हें कब क्या कार्य करना है। इससे कार्य में नियमितता आती है तथा सभी कार्यों को उचित महत्त्व प्रदान हो जाता है।
(4) कार्यों में नियमितता- समय-सारणी के द्वारा विद्यालय के समस्त कार्यों में नियमितता आती है, अस्त-व्यस्तता समाप्त होती है एवं अनुशासनहीनता खत्म होती है। समय-सारणी के द्वारा विभिन्न कार्यों में सामंजस्य स्थापित होता है। छात्र तथा अध्यापक दोनों को ही समय की उपलब्धता का ज्ञान रहता है। अतः वे अपने कार्यों को उसी हिसाब से करते हैं।
(5) थकान एवं शिथिलता में कमी- समय-सारणी किसी भी एक क्रिया को लम्बे समय तक नहीं होने देती। इससे एक ही कार्य को लम्बे समय तक करते रहने से ऊब तथा थकान से छुटकारा मिलता है। थोड़े समय पर क्रियाओं के बदल जाने से नीरसता समाप्त होती है। अच्छी सारणी में कठिन विषयों के बाद सरल विषयों के शिक्षण की व्यवस्था कर देने से भी थकान एवं शिथिलता कम होती है।
(6) नैतिक गुणों का विकास- समय-सारणी बालकों में अनेक नैतिक गुणों का विकास करती है। समय-सारणी से बालक व्यवस्थित कार्य करना सीखते हैं, वे समय के महत्त्व को जानने लगते हैं उनमें नियमितता आती है, अनेक कार्यों की सुनियोजित व्यवस्था करना सीखते हैं तथा वे विभिन्न साधनों एवं समय के बीच समन्वय स्थापित करना जानते हैं।
(7) अनुशासन स्थापना सम्भव- समय-सारणी के द्वारा बालकों तथा शिक्षक दोनों में ही अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिलती है। समय-सारणी के द्वारा बालकों तथा शिक्षकों को विभिन्न क्रियाओं में हर समय व्यस्त रखा जा सकता है।
(8) नियोजित शिक्षण सम्भव- समय-सारणी से शिक्षक तथा छात्र यह जान लेते हैं कि प्रत्येक विषय के अध्ययन-अध्यापन के लिए कितना समय दिया गया है। वे इसी हिसाब से शिक्षण को नियोजित करते हैं जिससे सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा किया जा सके।
(9) निरीक्षण की सुविधा- समय-सारणी के द्वारा अधिकारी जान लेते हैं कि किस् समय कौन-सा कार्य चल रहा है। इससे विभिन्न क्रियाओं का निरीक्षण करना सुविधाजनक रहता है।
(10) कार्य-वितरण में समानता-समय-सारणी से समस्त अध्यापकों के कार्य-भार में समता लाई जा सकती है। समान कार्य-वितरण सम्भव होता है। इससे उनमें मानसिक असन्तोष नहीं हो पाता है। समय-सारणी के द्वारा शिक्षकों को और भी अनेक लाभ हैं। इसके द्वारा उन्हें बीच-बीच में रिक्त कालांश देकर विश्राम का समय दिया जा सकता है जिससे उन्हें थकान न हो।
समय-सारणी निर्माण के सिद्धान्त
समय-सारणी निर्माण के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-
(1) विभागीय नियमों का पालन
समय-सारणी बनाते समय शिक्षा विभाग के विभिन्न नियमों का पालन करना चाहिए। किसी-किसी राज्य ने समय-सारणी से सम्बन्धित बडे व्यापक नियम दिये हैं। नियम हमें बताते हैं कि वर्ष में कितने दिन विद्यालय खुलेगा, किस विषय को कितना महत्त्व देना है तथा विद्यालय किस स्तर का है। प्राथमिक विद्यालय कम समय के लिये लगता है जबकि उच्चतर माध्यमिक अधिक समय के लिए। समय-सारणी बनाते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
(2) विषयों का काठिन्य
प्रत्येक विषय का कठिनाई-स्तर अलग होता है, कुछ विषय छात्रों के दृष्टिकोण से अधिक कठिन होते हैं और कुछ विषय अपेक्षाकृत अधिक सरल होते हैं। समय-सारणी बनाते समय विषयगत कठिनाई स्तर का ध्यान रखना चाहिए। कठिन विषयों को समय-सारणी में अपेक्षाकृत अधिक समय दिया जाय तथा उनका शिक्षण उस समय रखा जाय जब बालक कम थकान का अनुभव करते हैं और पढ़ने के लिए अधिक तत्पर रहते हैं।
(3) लचीलापन
समय-सारणी अधिक कठोर तथा स्थिर नहीं होनी चाहिए। बाद में उसमें कभी-कभी परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अतः समय-सारणी ऐसी बनाई जाय जिसमें कि आवश्यकता पड़ने पर सरलता से परिवर्तन किये जा सकें और इन भावी परिवर्तनों का विद्यालय की सम्पूर्ण व्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव न पड़े।
(4) साधनों की उपलब्धता
समय-सारणी बनाते समय सभी उपलब्ध मानवीय और भौतिकीय साधनों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक कक्ष, प्रयोगशाला भवन, उपकरण आदि सभी तथ्यों की उपलब्धता समय-सारणी को प्रभावित करती है अतः समय-सारणी के निर्माण के समय इन सबका ध्यान रखना चाहिए।
(5) थकान का ध्यान
समय-सारणी के निर्माण में बालकों तथा शिक्षकों की थकान का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ विषय अधिक थकान देते हैं जबकि कुछ विषय रोचक होते हैं। इसी प्रकार, विद्यालय समय में कुछ समय बालक ताजा रहते हैं तथा उनकी ग्रहणशीलता अच्छी रहती है। समय सारणी के निर्माण में इन सभी तथ्यों का बराबर ध्यान रखना चाहिए।
(6) मौसम का ध्यान
समय-सारणी निर्माण में मौसम सम्बन्धी तत्त्वों का भी ध्यान रखना पडता है। सामान्यतया यह स्वीकार किया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में कालाश छोटे होने चाहिए और शीत-ऋतु में कालांश अपेक्षाकृत कुछ बड़े होने चाहिए।
(7) शिक्षकों के हितों का ध्यान
समय-सारणी के निर्माण में शिक्षकों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। समय-सारणी में शिक्षकों की योग्यता, दक्षता एवं रुचि के अनुसार विषय दिये जाएँ, उन्हें बीच-बीच में खाली कालांश दिये जाएँ. उन्हें समान कार्य-भार दिया जाय तथा समय-सारणी निर्माण में अध्यापकों के साथ किसी भी बात का पक्षपात न किया जाय।
(8) व्यापकता
समय-सारणी व्यापक होनी चाहिए। उसमें सभी विषयों के आवश्यक उप-विषयों तथा अन्य सहगामी क्रियाओं की पूर्ण एवं स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। संक्षेप में समय सारणी अपने में पूर्ण होनी चाहिए।
(9) विभिन्नता का सिद्धान्त
समय-सारणी में विविधता तथा विभिन्नता लानी चाहिए। इससे तात्पर्य है कि प्रत्येक कालांश में विषयों की विविधता होनी चाहिए। दो समान प्रकृति के विषय लगातार दो कालांशों में न पढ़ाये जाएँ। यह सिद्धान्त प्रयोगात्मक कालांश पर लागू नहीं होता है। एक ही विषय के प्रयोगात्मक शिक्षण के लिए दो लगातार कालांश हो सकते हैं।