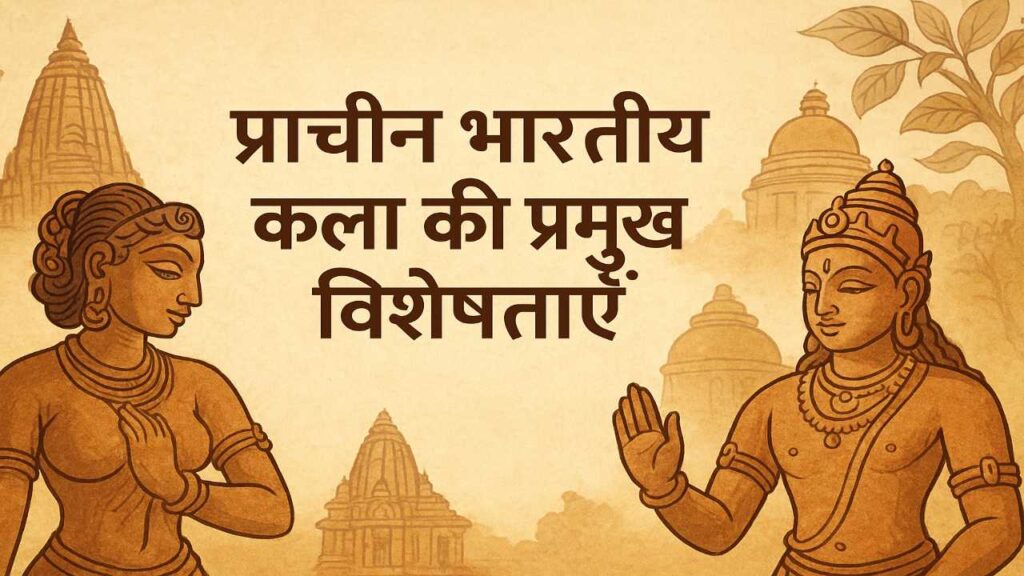इस लेख प्राचीन भारतीय कला की प्रमुख विशेषताएँ |Prachin Bharatiya Kala ki Pramukh Visheshataen में भारत की प्राचीन कला की उत्पत्ति, विकास और उसकी मुख्य विशेषताओं का विस्तार से विवेचन किया गया है। इसमें धर्म, आध्यात्मिकता, प्रतीकवाद, नारी सौंदर्य, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, और क्षेत्रीय शैलियों का वर्णन है। इसे पढ़कर हमें भारतीय कला की गहराई, विविधता, सौंदर्यबोध और उसके दार्शनिक तथा सांस्कृतिक महत्व का ज्ञान प्राप्त होता है।
Introduction
भारत विश्व की उन प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है जिसने कला के क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध परंपरा विकसित की। भारतीय कला केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं रही, बल्कि यह धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति का भी प्रमुख साधन रही है। यहाँ की कला ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष — धर्म, समाज, प्रकृति, लोक और जीवन-दर्शन — को स्पर्श किया है।
प्राचीन भारत में कला का विकास लगभग 3000 ई.पू. की सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्तकालीन स्वर्ण युग तक निरंतर हुआ। इस युग में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य तथा शिल्पकलाएँ अपनी पूर्णता तक पहुँचीं। भारतीय कला की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जीवन के आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों को मूर्त रूप दिया।
Prachin Bharatiya Kala ki Pramukh Visheshataen
प्राचीन भारतीय कला की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है-
भारतीय कला का धार्मिक आधार (Religious Foundation of Indian Art)
प्राचीन भारतीय कला का मूल आधार धर्म था। कला को पूजा का अंग माना गया। मंदिर, स्तूप, चैत्य, विहार, मूर्तियाँ, चित्र—all religious feelings के प्रतीक बने।
- वैदिक काल में अग्नि, सूर्य, वरुण जैसे देवताओं की प्रतीकात्मक चित्रण मिलता है।
- बौद्ध कला ने करुणा और शांति का संदेश दिया।
- जैन कला ने अहिंसा और त्याग की भावना को मूर्त रूप दिया।
- हिन्दू कला में देवताओं की मूर्तियाँ केवल पूजा के साधन नहीं रहीं, बल्कि उनके माध्यम से नैतिक और आध्यात्मिक संदेश प्रसारित किए गए।
इस प्रकार धर्म भारतीय कला का प्राणतत्व रहा, जिसने उसे गहराई और पवित्रता प्रदान की।
- खजुराहो के मंदिरों की स्थापत्य विशेषताएं | Khajuraho ke mandiro ki vishestaye B.A 3rd Year Notes
- रांके द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ और उनका महत्व B.A 3rd Year Notes
- टॉयनबी के अनुसार सभ्यता के उत्थान एवं पतन की प्रक्रिया B.A 3rd year Notes
- भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला का वर्णन
- हड़प्पा सभ्यता के नगर विन्यास(Town Planning) की प्रमुख विशेषताएँ
आध्यात्मिकता और प्रतीकवाद (Spiritualism and Symbolism)
भारतीय कला का दूसरा प्रमुख तत्व उसकी आध्यात्मिक दृष्टि है। कलाकार केवल भौतिक रूप से सुंदर वस्तु नहीं बनाता, बल्कि वह उसके भीतर छिपे ‘ब्रह्म’ या ‘सार तत्व’ को प्रकट करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए –
- बौद्ध कला में चक्र, पद्म (कमल), धर्मचक्र, वृक्ष, सिंहासन आदि प्रतीक रूप में बुद्ध की उपस्थिति दर्शाते हैं।
- हिन्दू मूर्तियों में त्रिशूल, शंख, चक्र, कमल, गरुड़, नंदी आदि प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं।
- भारतीय कलाकार के लिए कला ‘मायावी जगत’ नहीं बल्कि ‘आत्मा की झलक’ थी। इसलिए उसकी कला में भक्ति और ध्यान का स्वर मिलता है।
प्रकृति से गहरा संबंध (Intimate Relationship with Nature)
प्राचीन भारतीय कलाकार ने प्रकृति को अपनी प्रेरणा का स्रोत माना। वनस्पति, पशु-पक्षी, पर्वत, नदियाँ, मेघ, सूर्य, चंद्र—all तत्व भारतीय कला में बार-बार दिखाई देते हैं।
सिंधु सभ्यता के मोहरों पर पशु आकृतियाँ, वृक्ष पूजा, और नृत्य करती हुई स्त्रियाँ प्रकृति और जीवन का उत्सव प्रतीत होती हैं।
अजंता की भित्तिचित्रों में भी प्राकृतिक दृश्यों की मनोहारी प्रस्तुति है — वर्षा में भीगे वृक्ष, मयूर, कमल-सरोवर, पुष्प और लताओं से सजी चित्रकला भारतीय कलाकार की प्रकृति के प्रति अनुरक्ति को दर्शाती है।
मानव केंद्रित दृष्टिकोण (Human-Centric Approach)
यद्यपि भारतीय कला धार्मिक थी, फिर भी यह मानव केंद्रित रही। कलाकार ने मनुष्य को ईश्वर का प्रतिबिंब माना। इसलिए देवमूर्तियों में भी मानवीय भावनाओं का चित्रण मिलता है — जैसे मातृत्व, करुणा, वीरता, प्रेम, त्याग, ध्यान आदि। उदाहरणतः —
- अमरावती की मूर्तियों में स्त्रियों की कोमलता और सौंदर्य।
- गांधार कला में बुद्ध की मानवीय भाव-भंगिमा।
- गुप्तकालीन मूर्तियों में ‘मृदुल मुस्कान’ और ‘शांत मुखाभिव्यक्ति’।
इन सबमें कलाकार का उद्देश्य केवल देवत्व नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं की गरिमा दिखाना था।
आदर्शवाद और यथार्थवाद का संयोजन (Synthesis of Idealism and Realism)
भारतीय कला की एक विशेषता यह है कि इसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का सुंदर समन्वय मिलता है।
- सिंधु सभ्यता की नर्तकी में यथार्थवादी शरीर संरचना है, पर उसमें छिपा आत्मविश्वास आदर्श का रूप है।
- अजन्ता चित्रों में मानव आकृतियाँ यथार्थ में डूबी हुई हैं, पर उनके भाव आध्यात्मिक हैं।
- गुप्तकालीन मूर्तियाँ जैसे सारनाथ का बुद्ध, दिव्य और शांत आदर्श रूप है, किंतु उनका शारीरिक गठन यथार्थ के निकट है।
इस संयोजन ने भारतीय कला को अद्वितीय बनाया।
विविधता में एकता (Unity in Diversity)
भारत विविधताओं का देश है — भाषाएँ, धर्म, प्रदेश, जातियाँ — परंतु भारतीय कला ने इन सबको जोड़ने का कार्य किया। उत्तर भारत की गांधार कला, दक्षिण की अमरावती कला, मध्य भारत की सांची मूर्तिकला, पश्चिम की एलोरा गुफाएँ, पूर्व की पुरी कला — सबमें क्षेत्रीय विशेषताएँ हैं, फिर भी एक साझा भारतीय आत्मा विद्यमान है। यह “विविधता में एकता” भारतीय कला की आत्मा है।
नारी का सौंदर्य और मातृत्व भाव (Depiction of Femininity and Motherhood)
भारतीय कला में नारी को केवल सौंदर्य की प्रतिमा नहीं, बल्कि शक्ति, सृजन और मातृत्व की प्रतीक माना गया है।
- सिंधु सभ्यता की “नृत्य करती युवती” (Dancing Girl) में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता झलकती है।
- अमरावती और सांची की मूर्तियों में नारी का कोमल सौंदर्य, भावनाओं की गहराई और मातृत्व की गरिमा स्पष्ट दिखाई देती है।
- गुप्तकालीन मूर्तियों में पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा आदि देवी स्वरूप नारी की विविध भूमिकाओं का प्रतीक हैं — कभी सौंदर्य की देवी, कभी विद्या की अधिष्ठात्री, तो कभी शक्ति का रूप।
- अजंता की चित्रकला में स्त्रियाँ संगीत, नृत्य और प्रेम के भावों में तल्लीन दिखाई देती हैं — यह भारतीय कलाकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है।
भारतीय कलाकार ने नारी को ‘माया’ नहीं बल्कि ‘शक्ति’ के रूप में देखा, जो सृष्टि की आधारशिला है। यही कारण है कि भारतीय कला में नारी का स्थान अत्यंत पवित्र और आदरणीय रहा।
भावनात्मकता और रसानुभूति (Emotional Depth and Rasa Theory)
भारतीय कला केवल रूप-सौंदर्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने मानव भावनाओं के सूक्ष्मतम रूपों को भी व्यक्त किया। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित नौ रस — शृंगार, वीर, करुण, रौद्र, हास्य, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत — भारतीय कला की आत्मा हैं। चाहे अजंता की चित्रकला हो या खजुराहो की मूर्तिकला, प्रत्येक में किसी न किसी रस का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।उदाहरण के लिए —
- सारनाथ के बुद्ध की मूर्ति में “शांत रस” का उत्कर्ष है।
- अमरावती की यक्षिणियों में “शृंगार रस” की गहराई है।
- महाबलीपुरम के नृत्य दृश्यों में “वीर और अद्भुत रस” की छटा है।
भारतीय कला का उद्देश्य केवल आँखों को सुख नहीं देना था, बल्कि हृदय को भावनाओं से आंदोलित करना भी था। यही रसानुभूति भारतीय कला की गहराई को परिभाषित करती है।
लय, संतुलन और सामंजस्य (Rhythm, Balance and Harmony)
भारतीय कला में लयात्मकता और संतुलन का अद्भुत समन्वय मिलता है। मूर्तियों में शारीरिक मुद्रा, हाथों की गति, नेत्रों की दिशा, वस्त्रों की लहर—all में लय और गति का अदृश्य प्रवाह है।
चित्रकला में रंगों का सामंजस्य और वास्तुकला में स्थापत्य का संतुलन, दोनों ही ‘लय’ का साक्षात रूप हैं। उदाहरणतः —
- अजंता की चित्रों में रेखाओं की गति और रंगों का मेल ऐसा है मानो संगीत बह रहा हो।
- खजुराहो के मंदिरों में प्रत्येक मूर्ति अपनी स्थिति और मुद्रा में स्थापत्य से पूर्ण सामंजस्य रखती है।
यह सामंजस्य केवल बाह्य नहीं, बल्कि दार्शनिक भी है — जैसे सृष्टि में संतुलन है, वैसे ही कला में भी।
शिल्पकला और वास्तुकला का उत्कर्ष (Excellence of Architecture and Sculpture)
प्राचीन भारत में शिल्पकला और वास्तुकला का विकास अत्यंत उच्च स्तर पर हुआ। सिंधु सभ्यता में नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और ईंटों के घरों की संरचना विश्व में अद्वितीय थी। बौद्ध काल में स्तूप, विहार और चैत्य जैसे स्थापत्य रूप विकसित हुए — उदाहरणतः सांची स्तूप, भरहुत और अमरावती के शिल्प।
मौर्य काल में अशोक स्तंभ और पशु शीर्ष (जैसे सारनाथ का सिंहस्तंभ) भारतीय मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।गुप्तकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है — इस काल के मंदिर जैसे दशावतार मंदिर (देवगढ़) या उज्जैन का पार्श्वनाथ मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से अद्वितीय हैं।एलोरा और अजंता की गुफाओं में रॉक-कट (शैलखण्डीय) कला का चरम रूप दिखाई देता है। विशेषकर कैलाशनाथ मंदिर (एलोरा) एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है — यह तकनीकी और कलात्मक दोनों दृष्टियों से अनुपम है।
धर्मों का संगम (Fusion of Religious Streams)
भारतीय कला की एक अन्य विशेषता यह रही कि उसने विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय और सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया। बौद्ध, जैन और हिन्दू कला में अनेक विषय और प्रतीक समान हैं — जैसे कमल, चक्र, सिंहासन, वृक्ष, मंडल आदि। एलोरा गुफाओं में बौद्ध, जैन और हिन्दू — तीनों धर्मों के स्मारक एक ही परिसर में मिलते हैं। यह भारत की सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है।
भारतीय कलाकार का दृष्टिकोण विभाजनकारी नहीं था; वह सब धर्मों को एक ही सत्य की भिन्न अभिव्यक्तियाँ मानता था। इसीलिए भारतीय कला में धर्मों का संगम सौंदर्य और समरसता का प्रतीक बन गया।
प्रतीकात्मक और दार्शनिक दृष्टि (Philosophical and Symbolic Vision)
भारतीय कला का गूढ़ अर्थ उसके प्रतीकवाद और दर्शन में निहित है। उदाहरण के लिए —
- शिव का नटराज रूप सृष्टि, पालन और संहार के चक्र का प्रतीक है।
- विष्णु के शेषनाग पर विश्राम का अर्थ है — सृष्टि की स्थिरता और अनंतता। कमल का फूल निर्मलता और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है।
- बौद्ध धर्म में ‘धर्मचक्र’ ज्ञान और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक है।
इस प्रकार प्रत्येक आकृति, मुद्रा, और वस्तु केवल सौंदर्य का तत्व नहीं, बल्कि गहरे दार्शनिक अर्थ का वाहक है।
क्षेत्रीय शैलियों का विकास (Development of Regional Styles)
भारतीय कला ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट शैलियाँ विकसित कीं।
- गांधार कला: ग्रीक प्रभाव से प्रेरित — यथार्थवादी और मानव-केंद्रित।
- मथुरा कला: भारतीय परंपरा में जड़ित — आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक।
- अमरावती कला: बौद्ध कथाओं की सूक्ष्म और गतिशील प्रस्तुति।
- दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली: विशाल गोपुरम, मंडप और अलंकरणों से सुसज्जित।
- उत्तर भारत की नागर शैली: ऊँचे शिखर और सूक्ष्म मूर्तिकला कार्यों से युक्त।
ये सभी शैलियाँ मिलकर भारतीय कला की व्यापकता और विविधता को दर्शाती हैं।
लोककला और जनजीवन का प्रभाव (Influence of Folk and Daily Life)
भारतीय कला केवल राजाओं या धर्मों की अभिव्यक्ति नहीं रही, बल्कि लोकजीवन की सजीव झलक भी उसमें दिखाई देती है। अजंता के चित्रों में राजा, रानी, व्यापारी, संगीतज्ञ, नर्तक, पशु-पक्षी और सामान्य जनता — सभी का चित्रण मिलता है। सांची और भरहुत की मूर्तियों में ग्रामीण जीवन, कृषि कार्य, उत्सव, संगीत और नृत्य के दृश्य दिखाई देते हैं। यह लोक-संस्कृति की जीवंतता भारतीय कला की आत्मा को जनजीवन से जोड़ती है।
कला का नैतिक और शिक्षाप्रद उद्देश्य (Moral and Didactic Purpose of Art)
भारतीय कला केवल आनंद या मनोरंजन का माध्यम नहीं रही, बल्कि उसका उद्देश्य मानव को नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करना था।
मूर्तियाँ और चित्र केवल देवताओं के रूप नहीं, बल्कि धर्म, करुणा, संयम, त्याग और सत्य के प्रतीक भी थे।
उदाहरणतः —
- बुद्ध की मूर्तियाँ ध्यान और आत्मसंयम का संदेश देती हैं।
- जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ अहिंसा और तपस्या का प्रतीक हैं।
- हिन्दू देवताओं की कथाएँ कर्म, धर्म और मोक्ष के मार्ग की ओर संकेत करती हैं।
- इस प्रकार भारतीय कला का उद्देश्य “आनंद से अधिक अध्यात्म” रहा है।
कला और संगीत-नृत्य का संबंध (Interrelation of Art, Music and Dance)
भारतीय कला एक समग्र कला थी — जिसमें चित्र, मूर्ति, नृत्य, संगीत, वास्तु सब परस्पर जुड़े हुए थे। मंदिरों की दीवारों पर नर्तक-नर्तकियों की मूर्तियाँ, वाद्य यंत्रों के चित्र, और देवताओं के नृत्य रूप — यह सब इस समन्वय के प्रमाण हैं। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी जैसे नृत्य रूपों की मुद्राएँ और मंदिर मूर्तियों की मुद्राएँ एक-दूसरे से प्रेरित हैं। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में कला जीवन के हर रूप में प्रवाहित थी — दृश्य, श्रव्य और स्पर्शनीय सभी में।
भारतीय कला का वैश्विक प्रभाव (Global Influence of Indian Art)
भारतीय कला का प्रभाव केवल उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं रहा। गुप्तकाल और पश्चात् काल में भारतीय शिल्प और स्थापत्य की परंपरा दक्षिण-पूर्व एशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड तक पहुँची। अंगकोरवाट (कंबोडिया) का मंदिर, बोरोबुदुर (इंडोनेशिया) का स्तूप — इन सभी पर भारतीय कला की गहरी छाप है। यह भारतीय संस्कृति की विश्वव्यापकता और सार्वभौमिकता का प्रमाण है।
निष्कर्ष (Conclusion)
प्राचीन भारतीय कला केवल अतीत का गौरव नहीं, बल्कि आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसकी विशेषताएँ — धर्मनिष्ठा, आध्यात्मिकता, प्रतीकवाद, सौंदर्य, भावनात्मकता और नैतिकता — मानव सभ्यता की गहराई को दर्शाती हैं। यह कला केवल पत्थर, रंग या रेखाओं की नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है। भारतीय कला ने हमें यह सिखाया कि कला केवल देखने की वस्तु नहीं, जीने की साधना है। वह हमें सौंदर्य के माध्यम से सत्य की ओर, और रूप के माध्यम से आत्मा की ओर ले जाती है।